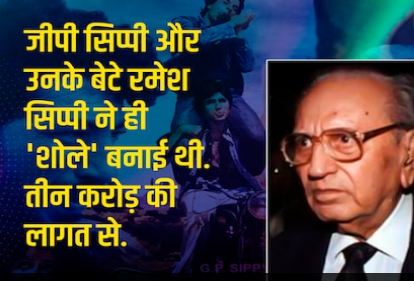दास्तान-गो : किस्से-कहानियां कहने-सुनने का कोई वक्त होता है क्या? शायद होता हो. या न भी होता हो. पर एक बात जरूर होती है. किस्से, कहानियां रुचते सबको हैं. वे वक़्ती तौर पर मौज़ूं हों तो बेहतर. न हों, बीते दौर के हों, तो भी बुराई नहीं. क्योंकि ये हमेशा हमें कुछ बताकर ही नहीं, सिखाकर भी जाते हैं. अपने दौर की यादें दिलाते हैं. गंभीर से मसलों की घुट्टी भी मीठी कर के, हौले से पिलाते हैं. इसीलिए ‘दास्तान-गो’ ने शुरू किया है, दिलचस्प किस्सों को आप-अपनों तक पहुंचाने का सिलसिला. कोशिश रहेगी यह सिलसिला जारी रहे. सोमवार से शुक्रवार, रोज़…
———–
जनाब, हिन्दुस्तान में पैसे कमाने वाली फिल्में तो बहुत हुईं हैं. लेकिन तारीख़ी तौर पर ‘नाम कमाने’ वाली कुछ चुनिंदा ही हो पाईं अब तक. ऐसी, जिन्हें फिल्मी दुनिया में ‘मील का पत्थर’ कहा जाए. मसलन- ‘मेरा नाम जोकर’, ‘मदर इंडिया’, ‘मुग़ल-ए-आज़म’, ‘शोले’ जैसीं. ये ऐसी फिल्में हुईं, जैसी न इनसे पहले बनीं और न बाद में. इनकी नक़लें करने की कोशिशें हुईं, पर हो न सकीं. सो, जाहिर तौर पर इन फिल्मों को बनाने वाले भी यूं नामचीन हुए कि हिन्दुस्तान की सरहदों से बाहर ‘हजारों-हजार कोस दूर तक’ उनकी पहचान बनी. भले इन लोगों ने कुछ गिनती की ही फिल्में क्यों न बनाई हों. मिसाल के तौर पर ‘शोले’ फिल्म का डायरेक्शन करने वाले रमेश सिप्पी और इसे बनाने वाले उनके वालिद जीपी सिप्पी, जिनका पूरा नाम था- गोपालदास परमानंद सिपाहीमलानी. कम लोग जानते होंगे, इन्हें इनके पूरे नाम से लेकिन काम (‘शोले’ जैसे) से सब वाक़िफ़ हैं.
साल 1914 के सितंबर महीने की 14 तारीख़ थी जनाब, जब जीपी सिप्पी हैदराबाद शहर में पैदा हुए. अंग्रेजों के ज़माने में, बंबई सूबे में सिंध का भी कुछ हिस्सा शामिल था. वहीं का हैदराबाद शहर, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है. इनका खानदान हिन्दुस्तान की आज़ादी से पहले तक वहीं रहा करता था. फिर कराची आया और बाद में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो ये लोग इस तरफ़ चले आए, हिन्दुस्तान. हालांकि, इनके जन्म के साल में कुछ असमंजस है. क्योंकि कहीं-कहीं 1913 या 1915 भी लिखा मिलता है. अलबत्ता, सही 2014 ही लगता है क्योंकि साल 2007 में 25 दिसंबर को जब जीपी सिप्पी साहब का इंतिक़ाल हुआ, तब इनकी उम्र 93 बरस बताई गई थी. इस सबके अलावा इनके सरनेम का भी एक मसला है. कहते हैं, अंग्रेज साहब लोगों को इनका सरनेम बोलने में दिक़्क़त हुआ करती थी. सो, उन्होंने सिपाहीमलानी को ‘सिप्पी’ कर दिया था.
तो जनाब, इस तरह जीपी सिपाहीमलानी हो गए आगे चलकर, जीपी सिप्पी. फिर जब हिन्दुस्तान को आज़ादी मिली तो सिर्फ़ मुल्क का नक्शा ही नहीं, दोनों तरफ के लाखों शरणार्थियों की तरह सिप्पी की भी पहचान बदलने को हुई. ये भी सिंध के अपने घर, अपनी ज़मीन, ज़ायदाद से उखड़ गए. पर चूंकि सिंधी क़ौम का खून रगों में था, तो सरहद के इस तरफ़ आने के बाद ज़्यादा परेशानी नहीं हुई. दो-तीन चीजों का आसरा था. एक तो बंबई में इनके पास पहले से कुछ ज़मीनें, वग़ैरा थीं. दूसरा, सरकार से भी पाकिस्तान में ज़मीन जायदाद छोड़ने के एवज़ में कुछ मुआवज़ा मिला था. तीसरा, जीपी सिप्पी साहब पढ़े-लिखे भी थे. वकालत की डिग्री थी इनके पास. हिन्दुस्तान के एक नामी वक़ील हुए, राम जेठमलानी साहब. वे और जीपी सिप्पी साहब, दोनों अच्छे दोस्त थे.
राम जेठमलानी के साथ काम कर चुके वकील विनायक बिछू ने एक बार बताया था, ‘सिंध से बंबई आए दोनों दोस्त चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे थे. दोनों की सरकारी वकील बनने की ख़्वाहिश थी. तभी रेलवे की अदालत में सरकारी वकील के ओहदे के लिए भर्ती भी हुई. इसमें जेठमलानी साहब चुने गए. लेकिन सिपाहीमलानी यानी सिप्पी साहब रह गए. इसके बाद जेठमलानी साहब ने वकालत के पेशे को ही आगे बढ़ाया मगर सिप्पी साहब ने इससे किनारा कर लिया. वे इमारतें बनाने का काम करने लगे’. यूं जनाब, जीपी सिप्पी साहब अब बंबई के कोलाबा, चर्चगेट जैसे इलाकों में जहां-जहां उनकी ज़मीनें थीं, उन पर इमारतें तानकर बेचने लगे. अब तक साल 1949 के आस-पास का वक़्त आ चुका था. इसी बीच, एक वाक़ि’आ हुआ और जीपी सिप्पी साहब फिल्मों में पैसे लगाने लगे. या कहें, फिल्में प्रोड्यूस करने लगे.
साल 1950 के आस-पास की बात है ये. जीपी सिप्पी साहब उस वक़्त बंबई के मरीन लाइंस इलाके में ‘गोविंद महल’ नाम की इमारत बना रहे थे. इसको बनाते-बनाते उन्हें उनके पारसी दोस्त फली मिस्त्री ने शायद, फिल्म बनाने का आइडिया दिया था. जीपी सिप्पी साहब ने भी इस बारे में संजीदगी से सोचा और इमारत बनाने के हुक़ूक़ (अधिकार) एक मुस्लिम बिल्डर को बेच दिए. उससे जो पैसा मिला, वह उन्होंने फली मिस्त्री के डायरेक्शन वाली फिल्म ‘सज़ा’ (1951) में लगा दिया. देवानंद और निम्मी ने इस फिल्म में अदाकारी दिखाई और यह ठीक-ठाक चल गई. इसके बाद तो जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 1997 (फिल्म ‘हमेशा’) तक बेरोक-टोक चलता रहा. इस दौरान जीपी सिप्पी साहब ने क़रीब दो दर्जन फिल्में बनाईं. आधा दर्जन के करीब फिल्मों का डायरेक्शन भी किया. और डायरेक्शन का सिलसिला शुरू करने में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लिया इन्होंन साल 1955 में ही जीपी सिप्पी साहब के डायरेक्शन की पहली फिल्म आ गई, ‘मरीन ड्राइव’. अंडरवर्ल्ड में चलने वाले तस्करी के धंधे पर कहानी लिखी गई थी. बीना राय और अजीत इसमें मुख्य अदाकार थे. अब तक सिप्पी साहब ‘सिप्पी फिल्म्स’ के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी बना चुके थे. इस बैनर ने हिन्द़ी फिल्मों की दुनिया को कई यादग़ार फिल्में दीं. जैसे, ‘अद्ल-ए-जहांगीर’ (1955), ‘श्रीमती 420’ (1956), ‘ब्रह्मचारी’ (1968), ‘अंदाज़’ (1971), ‘सीता और गीता’ (1972), ‘शान’ (1980), ‘सागर’ (1985), ’पत्थर के फूल’ (1991), वग़ैरा. और इन सबसे ऊपर ‘शोले’ (1975). यानी वह फिल्म जिसने हिन्दी फिल्मों की दुनिया में कई मायने बदल दिए.
‘शोले’ मतलब वह फिल्म जिसके एक-एक लाइन के डायलॉग (यहां इतना सन्नाटा क्यूं है भाई, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं) भी लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गए. वह फिल्म, जिसने छोटे-छोटे किरदार (सांभा, कालिया) करने वालों को भी हमेशा के लिए लोगों के ज़ेहन में बिठा दिया. वह फिल्म, जिसने डकैतों और उनकी ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली फिल्मी कहानियों को देखे जाने का नज़रिया ही बदल दिया. वह फिल्म, जो उस ज़माने में तीन करोड़ रुपए में बनी जब महज़ एक रुपया ख़र्च कर के तीन घंटे की पूरी फिल्म देख लिया करते थे. और तभी, इस फिल्म ने 1975 में ही, क़रीब 15 करोड़ रुपए कमा लिए थे. ‘शोले’ मतलब वह जिसे 2005 में 50वें फिल्मफेयर अवॉर्ड के दौरान ‘बीते 50 साल की सबसे अच्छी फिल्म’ माना गया. और यही वह फिल्म भी, जिसे 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने ‘हिन्दुस्तान की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों’ में शुमाार किया. कहां तक गिनाया जाए.
कुछ लफ़्ज़ों में कहें तो ‘शोले’ के नाम से ऐसा फिल्मी शाहकार सामने आया, जो कभी-कभार नुमूंदार होता है. लेकिन जब होता है तो कई दहाइयों, सदियों के लिए फ़लक पर ठहर सा जाया करता है. इसीलिए तो यह दास्तान शुरू करते वक़्त गब्बर सिंह के डायलॉग के अंदाज़ में थोड़ा रद्द-ओ-बदल कर के लिखा था कि ‘यहां (हिन्दुस्तान) से हजारों-हजार कोस दूर तक लोग जीपी सिप्पी को जानते हैं, क्योंकि? क्योंकि उन्होंने ‘शोले’ बनाई थी