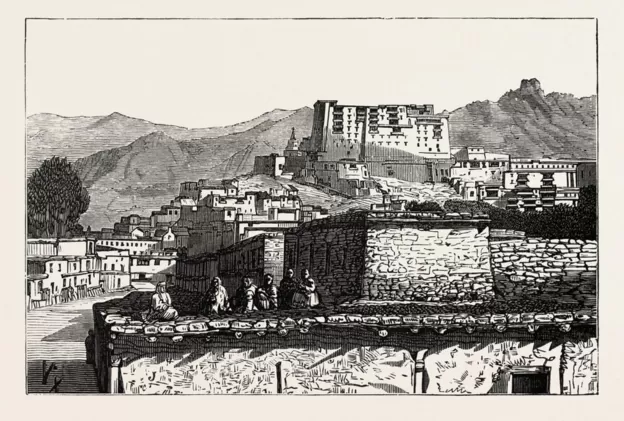आगमन की कहानी इतिहास से पहले मिथकों के रूप में शुरू होती है. ख्वाजा मोहम्मद आज़म दीदामरी नाम के सूफ़ी लेखक ने फारसी में ‘वाक़यात-ए-कश्मीर’ नाम से 1747 में एक किताब प्रकाशित की जिसकी कहानियां पौराणिक कथाओं की तर्ज़ पर लिखी गई थीं.
इसमें बताया गया है कि राक्षस जलदेव इस पूरे क्षेत्र को पानी में डुबोए रखता है. इस कहानी का नायक ‘काशिफ़’ है, जिसे वह किसी मारिची का बेटा बताता है. काशिफ़ महादेव की तपस्या करता है और फिर महादेव के सेवक ब्रह्मा और विष्णु जलदेव का दमन कर काशिफ़-सिर के नाम से इस क्षेत्र को रहने लायक़ बनाते हैं. विद्वान मानते हैं कि यह काशिफ़ वास्तव में कश्यप ऋषि की कहानी है, जिसमें घालमेल कर उसे जाने-अनजाने मुस्लिम जैसा साबित करने की कोशिश हुई है.
‘वाक़यात-ए-कश्मीर’ लिखने वाले आज़म के बेटे बदी-उद-दीन इस मिथकीय कहानी को और भी दूसरे स्तर पर लेकर चले गए. उन्होंने तो इसे सीधे आदम की कहानी से जोड़ दिया.
उनके मुताबिक़ कश्मीर में शुरू से लेकर 1100 साल तक मुसलमानों का शासन था जिसे हरिनंद नाम के एक हिंदू राजा ने जीत लिया. उनके मुताबिक़ कश्मीर की जनता को इबादत करना स्वयं हज़रत मूसा ने सिखाया. उनके मुताबिक़ मूसा की मौत भी कश्मीर में ही हुई और उनका मक़बरा भी वहीं है.
दरअसल, बदी-उद-दीन ने यह सब संभवतः शेख़ नूरुद्दीन वली (जिन्हें नुंद ऋषि भी कहा जाता है) के ‘नूरनामा’ नाम से कश्मीरी भाषा में लिखे गए कश्मीर के इतिहास पर आधारित करके लिख दिया. बहरहाल, इतिहासकारों ने चेरामन पेरूमल की कहानी की तरह इन कहानियों को भी कोई महत्व नहीं दिया है.
पृथ्वीनाथ कौल बामज़ई एक प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार हुए हैं. कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख़ अब्दुल्लाह ने उनसे कश्मीर का विस्तृत इतिहास लिखने का अनुरोध किया था.
1962 में प्रकाशित उनकी किताब ‘ए हिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर’ की भूमिका स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी. तीन खंडों में लिखित ‘कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ कश्मीर’ इस प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है.
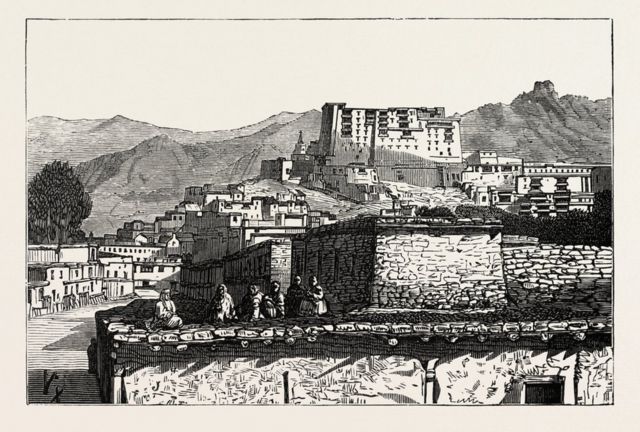
इस्लाम से कश्मीर का पहला परिचय
बामज़ई के मुताबिक़ मोहम्मद बिन-क़ासिम सिंध विजय के बाद कश्मीर की ओर बढ़े ज़रूर थे, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी. उनकी अकाल मृत्यु की वजह से उनका कोई दीर्घकालिक शासन भी स्थापित न हो सका. कश्मीर तक पहुंचने की दुर्गम भौगोलिक स्थिति की वजह से भी अरब वहां पहुंच पाने में असमर्थ रहे थे.
अरबों के साथ कश्मीरी हिंदू शासकों का पहला संपर्क कार्कोट राजवंश (625 से 885 ईस्वी) के दौरान हुआ था. मध्य एशिया और अफ़ग़ानिस्तान के अपने अभियानों के दौरान इस वंश के प्रमुख राजाओं जैसे चंद्रपीड़ और ललितादित्य का सामना अरबों से हुआ और पहली बार उनका परिचय इस्लाम नाम के इस नए धर्म से हुआ.
अरबों से उन्हें इतना ख़तरा महसूस हुआ कि ललितादित्य ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजकर मदद मांगी थी और अरबों के ख़िलाफ़ एक सैन्य गठबंधन बनाने का अनुरोध किया था.
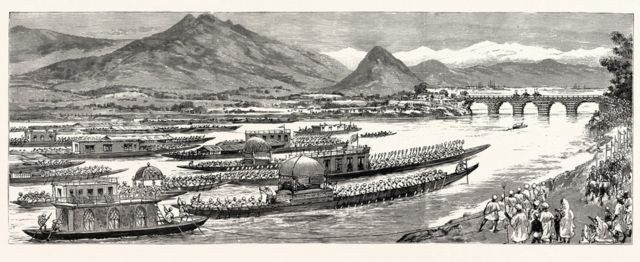
महमूद ग़ज़नी कभी कश्मीर को नहीं जीत सका
कश्मीर की दुरूह भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां किसी तरह का बाहरी घुसपैठ आसान नहीं था. इसके अलावा कश्मीर के राजा भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह बंद रखते थे और बाहरी संपर्क को हतोत्साहित करते थे.
1017 में भारत की यात्रा करने वाले अल-बेरूनी ने इस बारे में बहुत ही शिकायती लहजे में लिखा है- ‘कश्मीरी राजा ख़ास तौर पर अपने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं. इसलिए कश्मीर तक पहुंचने वाले हर प्रवेश-मार्ग और सड़कों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वे बहुत सावधानी बरतते हैं.”
“इस वजह से उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है. वे किसी ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देते जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते न हों.”
ध्यान रहे कि अल-बेरूनी का काल महमूद ग़ज़नी का काल भी है. भारत पर किए गए ग़ज़नी के कई आक्रमणों से हम परिचित हैं. ग़ज़नी से क़रीब सौ साल पहले काबुल में लल्लिया नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी जिसे इतिहासकार ‘हिंदू शाही’ कहते हैं. उन्होंने कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध क़ायम किए थे.
ग़ज़नी ने जब उत्तर भारत पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना. उस समय काबुल का राजा था जयपाल. जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी. मदद मिली भी, लेकिन वह ग़ज़नी के हाथों पराजित हुआ. पराजित होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचनपाल ने ग़ज़नी के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी.
त्रिलोचनपाल को तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्रामराजा (1003-1028) से मदद भी मिली, लेकिन वह अपना साम्राज्य बचा न सका. 12वीं सदी में ‘राजतरंगिणी’ के नाम से कश्मीर का प्रसिद्ध इतिहास लिखने वाले कल्हण ने इस महान साम्राज्य के पतन पर बहुत दुःख जताया है.
ग़ज़नी ने इसके बाद आज के हिमाचल का हिस्सा कांगड़ा भी जीत लिया, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य उनकी आंख का कांटा बना रहा. 1015 में उन्होंने पहली बार तोसा-मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला किया, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति और कश्मीरियों के ज़बरदस्त प्रतिरोध की वजह से उन्हें बहुत अपमान के साथ वापस लौटना पड़ा.
यह भारत में किसी युद्ध में उनके पीछे हटने का पहला मौक़ा था. वापसी में उनकी सेना रास्ता भी भटक गई और घाटी में आए बाढ़ में फंस गई. अपमान के साथ-साथ ग़ज़नी का नुक़सान भी बहुत हुआ.
छह साल बाद 1021 में अपने खोए हुए सम्मान को अर्जित करने के लिए ग़ज़नी से फिर से उसी रास्ते कश्मीर पर हमला किया. लगातार एक महीने तक उसने ज़बरदस्त प्रयास किया, लेकिन लौहकोट की क़िलाबंदी को वह भेद न सका. घाटी में बर्फ़बारी शुरू होने वाली थी और ग़ज़नी को लग गया कि इस बार उसकी सेना का हाल पिछली बार से भी बुरा होनेवाला है.
वह कश्मीर की अजेय स्थिति को भांप चुके थे. दोबारा अपमान का घूंट पीते हुए उन्हें फिर से वापस लौटना पड़ा. उसके बाद उन्होंने कश्मीर के बारे में सोचना भी बंद कर दिया.

कश्मीर के हिंदू राजा हर्षदेव पर इस्लाम का प्रभाव
उत्पाल वंश के राजा हर्षदेव या हर्ष ने 1089 से 1111 (कुछ विद्वानों के अनुसार 1038-1089) तक कश्मीर पर शासन किया. उनके बारे में माना जाता है कि वह इस्लाम से इस क़दर प्रभावित हो गए कि न केवल उन्होंने ख़ुद मूर्तिपूजा छोड़ दी, बल्कि कश्मीर में मौजूद मूर्तियों, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मंदिरों को भी ध्वस्त करने लगे.
इस काम के लिए उन्होंने ‘देवोत्पतन नायक’ नाम से एक विशेष पद का प्रावधान तक किया था. हर्ष ने अपनी सेना में तुरुष्क (तुर्क) सेनानायकों तक को नियुक्त किया था. ‘राजतरंगिणी’ के लेखक कल्हण उनके समकालीन थे. कल्हण के पिता चंपक को हर्ष का महामंत्री भी बताया जाता है. कल्हण ने मूर्तिभंजक हर्ष को अपमानजनक अंदाज़ में ‘तुरुष्क’ यानी ‘तुर्क’ की निंदात्मक उपाधि दी है.
1277 के आस-पास वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने कश्मीर में मुसलमानों की मौजूदगी बताई है. इतिहासकारों का मत है कि उस दौरान कश्मीर के बाहरी हिस्सों में और सिंधु नदी के आस-पास बसे दराद जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में धर्म-परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर रहे थे.
कश्मीर में इस्लाम का प्रचार तेज़ी से बढ़ रहा था और लोग इसे बड़ी संख्या में अपना रहे थे. इसका कारण था कि वहां की जनता वहां के राजाओं और सामंतों के आपसी झगड़े में पिस रही थी. ख़ासकर किसानों पर दोहरी मार पड़ रही थी.
एक तो उसे अपनी ज़मीन से कुछ भी उपज नहीं मिल पा रही थी, दूसरे एक-के-बाद-एक प्राकृतिक आपदाएं जैसे- सूखा, भूकंप, बाढ़ और आगलगी ने उनके जीवन को दुःख और निराशा से भर दिया था.
ठीक इसी दौर में उनका संपर्क मुस्लिम सैनिकों और सूफ़ी धर्म-प्रचारकों से होना शुरू हुआ. इस्लाम एक ऐसा नया विचार था, जो उनके मन में विश्वास और आशा का संचार कर पा रहा था. इस्लाम उन्हें सदियों पुराने शोषणकारी कर्मकांडों से भी निजात दिला रहा था. इसे हाथों-हाथ लिया गया.

कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक: एक तिब्बती बौद्ध
कश्मीर में इस्लाम के प्रसार के पूरे कालक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उसे अपना पहला मुस्लिम शासक मिला. एक ऐसा मुस्लिम शासक जो वास्तव में एक तिब्बती बौद्ध थे और जिनकी रानी एक हिंदू थी.
1318 से 1338 के बीच के बीस साल कश्मीर में भारी उथल-पुथल के रहे. इस दौर में युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और मार-काट का बोलबाला रहा. लेकिन इससे ठीक पहले के बीस साल यानी 1301 से 1320 तक राजा सहदेव के शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में कश्मीर की जनता सूफ़ी धर्म-प्रचारकों के प्रभाव में और इन कारणों से इस्लाम को स्वीकार कर चुकी थी. अब उसे अपना पहला मुस्लिम शासक भी मिलने ही वाला था.
बामज़ई सहित कई इतिहासकारों ने इस महत्वपूर्ण प्रकरण का विस्तार से वर्णन किया है. इस कहानी के केंद्र में तुर्किस्तान से आया एक सूफ़ी धर्म-प्रचारक है. इनका सबसे प्रचलित नाम बुलबुल शाह था जबकि इतिहासकारों ने कई अलग-अलग नामों से इनका वर्णन किया है जिनमें से कुछ नाम हैं- सैय्यद शरफ़-उद-दीन, सैय्यद अब्दुर्रहमान. बामज़ई ने एक स्थान पर इनका नाम बिलाल शाह भी बताया है.
बुलबुल शाह सुहरावर्दी मत के सूफ़ी ख़लीफ़ा शाह नियामतुल्लाह वली फारसी के शिष्य थे. बुलबुल शाह ने कई देशों की यात्रा की थी और बग़दाद में काफ़ी समय बिताया था. इनका निजी जीवन और संवाद का तरीक़ा कश्मीरी लोगों को बहुत प्रभावित करता था. इन्होंने कश्मीर की पहली यात्रा राजा सहदेव के समय ही की थी.
सहदेव एक कमज़ोर शासक थे और वास्तव में उनके नाम पर उनके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र ही वास्तविक शासन चला रहे थे. रामचंद्र की सुंदर और मेधावी बेटी कोटा भी इस काम में उनकी मदद करती थी.
इसी दौरान तिब्बत से भागा हुआ एक राजकुमार रिंचन या रिनचेन (पूरा नाम लाचेन रिग्याल बू रिनचेन) कुछ सौ सशस्त्र सैनिकों के साथ कश्मीर पहुंचा. रिंचन के पिता तिब्बती राजपरिवार और कालमान्य भूटियाओं के बीच छिड़े गृहयुद्ध में मारे जा चुके थे, लेकिन रिंचन अपनी जान बचाकर ज़ोजिला दर्रे के रास्ते कश्मीर की ओर भागने में सफल रहे थे. रामचंद्र ने रिंचन को शरण दी.
इसी बीच स्वात घाटी से शाह मीर नाम का एक मुस्लिम सेनानायक भी अपने परिवार और सगे-संबंधियों के साथ कश्मीर पहुंचे. उन्हें किसी फ़क़ीर ने कहा था कि वह एक दिन कश्मीर के शासक बनेंगे. वह अपने इसी सपने को साकार करने यहां पहुंचे थे. रामचंद्र और सहदेव ने उन्हें भी शरण दे दी. इस तरह अब रामचंद्र, कोटा, रिंचन और शाह मीर मिलकर कश्मीर का शासन देखने लगे.

उसी दौरान मध्य एशिया के एक तातार शासक दुलचु ने झेलम घाटी के रास्ते कश्मीर पर आक्रमण कर दिया. लड़ने की बजाय राजा सहदेव भागकर किश्तवाड़ चले गए. दुलचु ने आठ महीने तक कश्मीर में भयंकर उत्पात मचाया. रसद के अभाव में वह दर्रों के रास्ते भारत के मैदानी हिस्सों की ओर चल पड़े, लेकिन बर्फीले तूफ़ान में फंसकर वह और उनके हज़ारों सैनिक मारे गए.
अब शासन की बागडोर रामचंद्र ने संभाल ली. दुलचु ने कश्मीर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. रामचंद्र को राजा बनते देख रिंचन की भी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उन्होंने मौक़ा देखकर विद्रोह कर दिया. उनके आदमियों ने धोखे से रामचंद्र की हत्या कर दी, अब रिंचन ख़ुद कश्मीर की गद्दी पर क़ाबिज़ हो गए. कोटा के सामने कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने बहुत मनुहार के बाद मन मारकर रिंचन से विवाह कर लिया. रिंचन ने कोटा के भाई यानी रामचंद्र के बेटे रावणचंद्र को भी शासन में प्रमुख स्थान देकर संभवतः उसे सेनापति नियुक्त किया.
लेकिन रिंचन अब भी ख़ुद को लामा ही मानते थे जबकि कोटा रानी चाहती थी कि वह हिंदू बन जाएं. रिंचन के समक्ष भी कश्मीरी जनता से वैधता हासिल करने की चुनौती थी ही. वह एक बार को हिंदू धर्म अपनाने को राज़ी भी हो गए.
लेकिन यह इतना आसान नहीं था. कहा जाता है कि उस समय के कश्मीरी शैव गुरु ब्राह्मण देवस्वामी ने उन्हें हिन्दू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया. इसके कम-से-कम तीन कारण गिनाए जाते हैं-
पहला कि रिनचेन तिब्बती बौद्ध थे.
दूसरा कि वह अपने श्वसुर और एक हिन्दू राजा रामचंद्र के हत्यारे थे.
और तीसरा कि यदि उन्हें हिन्दू धर्म में अपनाया जाता तो उन्हें उच्च जाति में शामिल करना पड़ता.
आख़िरकार हार कर उन्होंने इस्लाम धर्म क़बूल कर लिया. कई विद्वान उनके इस्लाम धर्म अपनाने के पीछे मुस्लिम बहुल होती जा रहे रियासत में उनकी राजनीतिक सुरक्षा और महत्वाकांक्षा भी बताते हैं.
सचाई जो भी हो, इस्लाम में दीक्षित होने के बाद रिंचन को बुलबुल शाह ने ‘सदर-उद-दीन’ का नाम दिया. इस तरह वह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने. सदर-उद-दीन का अर्थ है- धर्म (इस्लाम) का मुखिया.
बुलबुल शाह ने जल्दी ही मारे गए राजा रामचंद्र के भाई रावणचंद्र को भी इस्लाम में दीक्षित कर लिया. शासन के कई उच्चाधिकारी भी बुलुबुल शाह के प्रभाव में इस्लाम में दीक्षित हुए. वहीं रिंचन के साथ आए तिब्बती भी इस्लाम में दीक्षित हुए. इस तरह बुलबुल शाह एक प्रकार से इस्लाम को कश्मीर का राजकीय धर्म बनाने के अपने मिशन में सफल रहे.
श्रीनगर के पांचवे पुल के नीचे कश्मीर की पहली मस्जिद भी रिंचन ने ही बनवाई. उस स्थान को अब भी बुलबुल लांकर कहा जाता है. 1327 में जब बुलबुल शाह की मृत्यु हुई तो उन्हें उसी मस्जिद के पास दफ़नाया गया. बुलबुल शाह को कई बार ‘बुलबुल-ए-कश्मीर’ के रूप में भी याद किया जाता है.
रिंचन की मृत्यु जल्दी ही हो गई. लेकिन इसके बाद कश्मीर ने इस्लामी सल्तनत का एक पूरा दौर देखा. इतना सबके बावजूद कश्मीरी अवाम में ‘इस्लामियत’ जैसी चीज़ कभी देखने को नहीं मिली. उसकी एक कहानी अलग से लिखी जा सकती है.

जिस तरह भारतीय इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम के नज़रिए से देखने-दिखाने वाला नैरेटिव झूठा है. ठीक उसी तरह कश्मीर घाटी के वे तंज़ीम जो इस्लाम को कश्मीरियत का एक्सक्लूसिव और अनिवार्य घटक मानते हैं, वह भी एक प्रकार का छलावा है. ठीक इसी तरह शेष भारत में भी कश्मीरियों के प्रति फैल चुका और फैलाया जा रहा धर्मोन्मादी पूर्वाग्रह बेबुनियाद है.
हाल में कश्मीर के ऊपर लिखी गई बहुचर्चित पुस्तक ‘कश्मीरनामा’ के लेखक अशोक कुमार पांडेय ने इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात कही है. उन्होंने लिखा है― ‘कश्मीर मानस का निर्माण बौद्ध, कश्मीर शैव तथा इस्लाम की सूफ़ी परम्पराओं के समन्वय से निर्मित हुआ है और इसके प्रभाव वहां के सामाजिक-राजनीतिक जीवन पर स्पष्ट हैं.’
हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि एक तरफ़ कश्मीर में दोनों समुदायों के अंतर्विरोधों पर पर्दा डालकर कश्मीरियत का आभासी संसार प्रदर्शित करना या फिर दूसरी तरफ़ इसे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के इकलौते रंग में देखना, ये दोनों ही अतिरेकी आयाम घातक हैं.
पांडेय ने लिखा है- ‘बौद्ध, शैव और सूफ़ी इस्लाम के मिश्रण से जो एक विशिष्ट कश्मीरी संस्कृति बनी है उसे समझने के लिए बहुत उदार और गहन दृष्टि की आवश्यकता है.’
अफ़सोस कि देश भर में वह उदार और गहन दृष्टि पैदा करने में हम फिलहाल बुरी तरह नाकाम होते दिख रहे हैं. इतिहास को पलटना और दिखाना कई बार इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है.